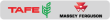शालिनी अग्रवाल
जयपुर। भारत के सबसे बड़े शहर एक ऐसे संकट का सामना कर रहे हैं जो हर दिन और गहराता जा रहा है। भीड़भरी सड़कों और ऊंची इमारतों के नीचे की जमीन धीरे-धीरे धंस रही है। वर्जीनिया टेक विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि यह धीमा धंसाव इमारतों को कमजोर कर रहा है और लाखों लोगों की जान को खतरे में डाल रहा है।
शोध क्या कहता है
यह अध्ययन नेचर सस्टेनेबिलिटी नामक जर्नल में प्रकाशित हुआ है। इसमें भारत के पांच बड़े महानगरों, नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और बेंगलुरु की जमीन का 2015 से 2023 तक सैटेलाइट डेटा से अध्ययन किया गया। वैज्ञानिकों ने पाया कि करीब 878 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की जमीन धंस रही है। लगभग 19 लाख लोग ऐसे इलाकों में रह रहे हैं जहां जमीन हर साल 4 मिलीमीटर से ज्यादा नीचे जा रही है। इसका मुख्य कारण है भूजल (groundwater) का अत्यधिक दोहन।
वर्जीनिया टेक की सहायक प्रोफेसर सुज़ाना वर्थ ने बताया, “जब शहर प्रकृति की क्षमता से ज्यादा पानी जमीन के अंदर से निकालते हैं, तो जमीन सचमुच नीचे धंसने लगती है।”
कैसे होता है धंसाव
जब भूजल निकाला जाता है, तो मिट्टी के अंदर मौजूद खाली जगहें सिकुड़ जाती हैं और ऊपर की सतह धीरे-धीरे नीचे चली जाती है। मानसून के बदलते पैटर्न से यह समस्या और बढ़ गई है, क्योंकि अब बारिश का पानी पहले की तरह जमीन में नहीं उतर पाता। सैटेलाइट आंकड़े यह भी दिखा रहे हैं कि भारत में कुल जल भंडार लगातार घट रहा है, यह कमी अब अंतरिक्ष से भी देखी जा सकती है।
हर शहर की अपनी कहानी
शोधकर्ताओं ने यह भी संकेत दिया कि ऊंची इमारतों और भारी निर्माणों का वजन भी जमीन को और नीचे धकेल रहा है।
असमान धंसाव और इमारतों पर असर
समस्या यह नहीं कि जमीन सिर्फ नीचे जा रही है, बल्कि वह असमान रूप से धंस रही है। इसे डिफरेंशियल सेटलमेंट कहा जाता है। इससे इमारतों की नींव झुकने लगती है, दीवारों में दरारें आती हैं और पाइपलाइनें टूट जाती हैं। मुख्य शोधकर्ता नितेशनिर्मल सदाशिवम के अनुसार, “आज जो मौन दबाव दिख रहा है, वह कल के बड़े हादसों में बदल सकता है, अगर शहरों ने अपनी नीतियों में बदलाव नहीं किया।”
सैटेलाइट से निगरानी
शोधकर्ताओं ने जमीन की हलचल को पकड़ने के लिए InSAR (Interferometric Synthetic Aperture Radar) तकनीक का इस्तेमाल किया। इससे मिलीमीटर तक की सटीकता से पूरे शहर की जमीन में हो रहे बदलाव का नक्शा तैयार किया गया।लगभग 1200 रडार तस्वीरों से यह पता चला कि छोटे-छोटे बदलाव समय के साथ मिलकर बड़ी संरचनात्मक कमजोरियां पैदा कर रहे हैं। दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में करीब 2400 इमारतें पहले से ही खतरे में हैं। अगर कुछ नहीं किया गया, तो अगले 50 सालों में 23 हजार से ज्यादा इमारतें गंभीर जोखिम में होंगी।
आने वाले खतरे
चेन्नई सबसे अधिक जोखिम में है, इसके बाद दिल्ली और मुंबई का नंबर आता है। एक बार नींव में दरार आने के बाद उसे भरना लगभग असंभव होता है। जमीन का असमान धंसाव जल निकासी व्यवस्था और पाइपलाइन को भी बिगाड़ देता है, जिससे बाढ़ और जलभराव का खतरा बढ़ता है।
जलवायु परिवर्तन से और संकट
सूखा, अनियमित मानसून और तेज़ी से बढ़ता शहरीकरण इस समस्या को और गहरा बना रहे हैं। सूखे में जब शहर अधिक पानी निकालते हैं, तो जमीन कमजोर होती जाती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि दुनिया के 150 से ज्यादा शहरी क्षेत्र पहले से ही इसी तरह की स्थिति का सामना कर रहे हैं।
समाधान क्या है
वर्जीनिया टेक के प्रोफेसर मनुशेर शिर्जाई के शब्दों में, “अगर हम आज अनुकूलन में निवेश करेंगे, तो भविष्य में जान और संसाधन दोनों बचाए जा सकेंगे।” यह चेतावनी केवल भारत के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के सभी शहरों के लिए है — क्योंकि जब धरती संतुलन खोती है, तो वह किसी की नहीं सुनती।
Published on:
30 Oct 2025 04:56 pm
बड़ी खबरें
View Allखास खबर
ट्रेंडिंग