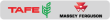रिजर्व बैंक ने बुधवार को जिस व्यापक सुधार पैकेज की घोषणा की है, वह न केवल बैंकिंग क्षेत्र की दिशा बदलने वाला है, बल्कि कॉर्पोरेट ऋण, पूंजी बाजार और वित्तीय पारदर्शिता की पूरी संरचना को नया आकार देगा। एक दशक से अधिक समय बाद रिजर्व बैंक ने ऐसा बड़ा कदम उठाया है, जिसमें बैंकों को अधिक लचीलापन, कंपनियों को सस्ता ऋण और पूंजी बाजार को नई ऊर्जा देने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रुपए को मजबूत करने का स्पष्ट संदेश नजर आ रहा है। इन उपायों का मुख्य उद्देश्य 10,000 करोड़ रुपए से अधिक के बैंक ऋण वाली कंपनियों के लिए ऋण के नियमों को आसान बनाना है, जिसमें पिछली सीमा और अतिरिक्त पूंजी आवश्यकताओं को हटा दिया गया है, जिससे ऋण देना महंगा हो गया था।
नए सुधारों का सबसे बड़ा लाभ यह है कि ऋण की पहुंच का विस्तार होगा। आइपीओ फाइनेंसिंग की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए और शेयरों पर ऋण सीमा 20 लाख से बढ़ाकर एक करोड़ रुपए कर दी गई है। सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों (लिस्टेड डेट सिक्योरिटीज) पर ऋण की सीमा हटाना एक और साहसिक कदम है, जिससे निवेशकों और कंपनियों दोनों को नया सहारा मिलेगा। अब तक भारतीय बैंक कॉर्पोरेट अधिग्रहण या इक्विटी-आधारित फाइनेंसिंग से दूरी बनाए रखते थे। इस कारण भारतीय कंपनियों को महंगे एनबीएफसी, प्राइवेट इक्विटी फंडों या विदेशी कर्जदाताओं पर निर्भर रहना पड़ता था। इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय बैंकिंग क्षेत्र अधिग्रहण वित्तपोषण की वैश्विक दौड़ से पिछड़ गया। दो दशक के अंतराल के बाद नए शहरी सहकारी बैंकों के लिए लाइसेंसिंग फिर शुरू करना भी महत्त्वपूर्ण है। यह कदम छोटे शहरों और कस्बों में बैंकिंग पहुंच को बढ़ाएगा और वित्तीय समावेशन को मजबूत करेगा। इस सुधार पैकेज को केवल बैंकिंग या वित्तीय क्षेत्र की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। यह भारतीय अर्थव्यवस्था की गति, पूंजी बाजार की गहराई और वैश्विक प्रतिस्पर्धा, खासकर 'ट्रंप टैरिफ' के बाद उत्पन्न हुए आर्थिक परिदृश्य में देश की स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था को अगले दशक में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की आधारशिला साबित हो सकता है।
हालांकि, इन सुधारों के साथ जोखिम भी जुड़े हुए हैं। लीवरेज्ड बायआउट जैसे मॉडल पश्चिमी देशों में सफल रहे हैं, लेकिन उनके साथ डिफॉल्ट और वित्तीय संकट के खतरे भी रहे हैं। 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट की जड़ें भी आंशिक रूप से आक्रामक अधिग्रहण वित्तपोषण से जुड़ी थीं। इसलिए, भारतीय संदर्भ में यह आवश्यक है कि निगरानी और जोखिम प्रबंधन के सख्त ढांचे लागू हों। यदि इन सुधारों को अविवेकपूर्ण तरीके से लागू किया गया तो परिणाम उल्टा भी हो सकता है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि अलग-अलग बैंकों के स्तर पर ऋणों की निगरानी जारी रहेगी और आवश्यकता पडऩे पर प्रणालीगत सुरक्षा उपाय अपनाए जाएंगे। यह भरोसा दिलाता है कि सुधारों के साथ-साथ विवेक भी बरता जाएगा।
Published on:
02 Oct 2025 08:17 pm
बड़ी खबरें
View Allओपिनियन
ट्रेंडिंग