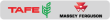हम हर दिन टैक्स देते हैं, सड़कें, अस्पताल, स्कूल समेत नागरिक सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं। शासन की व्यवस्थाओं और सूबे की संस्थाओं पर भरोसा करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह भरोसा कितना वास्तविक है? 19 सितंबर 2025 को फेडरल हाईकोर्ट के जस्टिस अमित रावल को जोधपुर से रणथम्भौर जाते समय राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक भी सार्वजनिक शौचालय नहीं मिला। शौचालय की तलाश में तेज गाड़ी चलाने के कारण चार चालान कट गए। यह सिर्फ एक जज की परेशानी नहीं थी- यह लाखों नागरिकों की रोजमर्रा की जद्दोजहद है। उन्होंने अदालत में इस बात को गंभीर चेतावनी के साथ पेश किया। इसी तरह, 25 जुलाई 2025 को झालावाड़ जिले के पिपलोदी गांव में सरकारी स्कूल की छत गिरने से सात बच्चों की मौत हो गई। राजस्थान हाईकोर्ट ने इसे स्वत: संज्ञान में लिया और राज्यभर के 86,000 से अधिक जर्जर क्लासरूम्स को बंद करने का आदेश दिया।
ये घटनाएं स्पष्ट करती हैं कि न्यायपालिका केवल कानून लागू करने वाली संस्था नहीं, बल्कि आम जनता की सुरक्षा, गरिमा और अधिकारों की रक्षक भी है। विशेषज्ञों का मानना है कि न्यायपालिका का काम केवल कानून लागू करना ही नहीं है, बल्कि समाज में व्याप्त समस्याओं का गहन अवलोकन करना भी है। यदि न्यायाधीश समय-समय पर सीधे जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं का अनुभव लें, तो न केवल उनके न्यायिक निर्णयों में व्यावहारिक दृष्टिकोण बढ़ेगा, बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 हर नागरिक को ‘जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता’ का अधिकार देता है। इसका दायरा केवल अस्तित्व तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता और शांतिपूर्ण जीवन का अधिकार भी शामिल है। जब शासन-प्रशासन इन अधिकारों की अनदेखी करता है, तब न्यायपालिका स्वत: संज्ञान या जनहित याचिका के माध्यम से हस्तक्षेप करती है। उदाहरण के तौर पर, राष्ट्रीय राजमार्ग पर सार्वजनिक शौचालय का अभाव सीधे अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 47 (जनस्वास्थ्य बढ़ाना राज्य का कर्तव्य) से जुड़ा है। वहीं, झालावाड़ स्कूल हादसा अनुच्छेद 21-ए (शिक्षा का अधिकार) और अनुच्छेद 39(एफ) (बच्चों की सुरक्षा) का उल्लंघन था।
दुनिया के कई देशों में जनहित याचिका और स्वयं संज्ञान जैसी न्यायिक सक्रियता मौजूद है, लेकिन इसका तरीका और असर अलग-अलग होता है। अमेरिका में इसके समक्ष ‘क्लास एक्शन मुकदमे’ और ‘सिटीजन स्यूट्स’ हैं, जिनके जरिए नागरिक या गैर सरकारी संस्थान सरकार या बड़ी संस्थाओं के खिलाफ पर्यावरण, उपभोक्ता संरक्षण या नागरिक अधिकारों के उल्लंघन पर केस कर सकते हैं, लेकिन अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट आमतौर पर स्वयं किसी मामले पर संज्ञान नहीं लेता और केवल दायर किए गए मामलों की सुनवाई करता है। वहीं, ब्रिटेन में ‘ज्यूडिशियल रिव्यू’ का प्रावधान है। इसके तहत नागरिक या गैर सरकारी संस्थान यह जांच सकते हैं कि सरकारी निर्णय कानून के अनुसार हुए हैं या नहीं। यहां अदालत केवल सरकारी कार्यों की वैधता पर हस्तक्षेप करती है और नीति बदलने का अधिकार आमतौर पर नहीं रखती। ब्रिटेन में भी न्यायपालिका आमतौर पर खुद कोई मामला शुरू नहीं करती, बल्कि केवल तब हस्तक्षेप करती है जब कोई औपचारिक याचिका दायर की जाती है। भारत में जनहित याचिका ने न्यायिक प्रणाली में गहरा हस्तक्षेप किया है। इसकी नींव पहली बार 1976 में मुंबई कामगार सभा बनाम अब्दुलभाई फैज़ुल्लाभाई [1976 (3) एससीसी 832] में जस्टिस कृष्णा अय्यर ने रखी। इसके बाद जस्टिस पी. एन. भगवती के प्रयासों से जनहित याचिका विकसित हुई और यह नागरिक अधिकारों की रक्षा का एक शक्तिशाली साधन बन गई।
एक स्वस्थ लोकतंत्र में संसद कानून बनाती है और कार्यपालिका उसे लागू करती है। लेकिन जब ये दोनों विफल हो जाते हैं, न्यायपालिका नागरिकों का अंतिम सहारा बनती है। जनहित याचिका और स्वत: संज्ञान न्यायपालिका, प्रशासन और नागरिकों के बीच संवाद और जवाबदेही का तंत्र मजबूत करते हैं। जब जज अपने अनुभव साझा करते हैं और प्रशासनिक संस्थाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो यह समाज में सकारात्मक बदलाव की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। न्यायपालिका का समय पर हस्तक्षेप लोकतंत्र की आत्मा को जीवित रखता है।
Published on:
25 Sept 2025 05:01 pm
बड़ी खबरें
View Allओपिनियन
ट्रेंडिंग